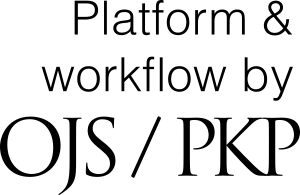21वीं शताब्दी का रंगमंच:
DOI:
https://doi.org/10.8855/wqr06669Abstract
21वीं शताब्दी अपने आप में एक विशिष्ट सदी है । जो निरंतर प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील के पथ पर अग्रसर है । इस युग का साहित्य में विशेष स्थान है । वहीं नवीन आविष्कारों से नाटकों की मूलभूत अवधारणा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं । नवीन मंच अभिकल्पन, प्रयोगशील रंग अन्वेषण, शब्द रस के अनुसंधन, आधुनिक प्रासंगिकता में संचार के प्रचार प्रसार के महाविस्फोट का युग है । नाटक और रंगमंच ग्लोबल मनुष्य और उसकी अस्मिता के केन्द्र में है । वैश्विक परिदृश्य हमारे भीतर पसर गया है । ”बाजारवाद मन की रंगभूमि को बंजर बना रहा है । शब्द बंधुआ हो गये हैं । वैचारिक स्वराज्य मरणासन्न एवं बंधक हैं । सत्ता का गणित चेहरे विहीन समाज की ओर धकेल रहा है“ । नाटकों की कथावस्तु में यथार्थता का गुण आ गया है ।जैसे प्रसाद युग में आदर्शवादी कथावस्तु होती थी । वर्तमान में वह बदलकर यथार्थवादी हो गयी है जो मानव जीवन के सर्वाधिक करीब है । आधे अधूरे (मोहन राकेश) 21वीं शताब्दी के पहले दशक में जहाँ नई पीढ़ी के नाट्क सृजकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वहीं नवीन आविष्कारों से नाटकों की मूलभूत अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए है । पात्रों के संवादों और अभिनय में परिवर्तन आया है । पात्रों के परिधान, अलंकार, भाव-भंगिमा आदि का प्रकटीकरण रंगमंच पर अच्छी प्रकार से संभव है । ”जिस प्रकार रंगमंच को जीवित और सक्रिय रखने के लिए नाटक की निरंतर रचना होती है, उसी प्रकार रंगमंच सजीव होने से समर्थ लेखक नाटक को अपनी अनुभूति के व्यापक और विस्तृत से प्रेषण का माध्यम पाता है और सहज ही उसका उपयोग करने को उन्मुख होता है । रंगमंच सक्रिय होने से लेखक का नाट्यात्मक अनुभूति से निरंतर साक्षात्कार होता रहता है जिससे नाटककार के रूप में उसके सृजनात्मक व्यक्तित्त्व के निर्माण और विकास में सहायता मिलती है ।“ अर्थात् नाटक की सर्जना रंगमंच और मंच की सृजना नाटक (रंग) के लिए अति आवश्यक मानी गई है ।